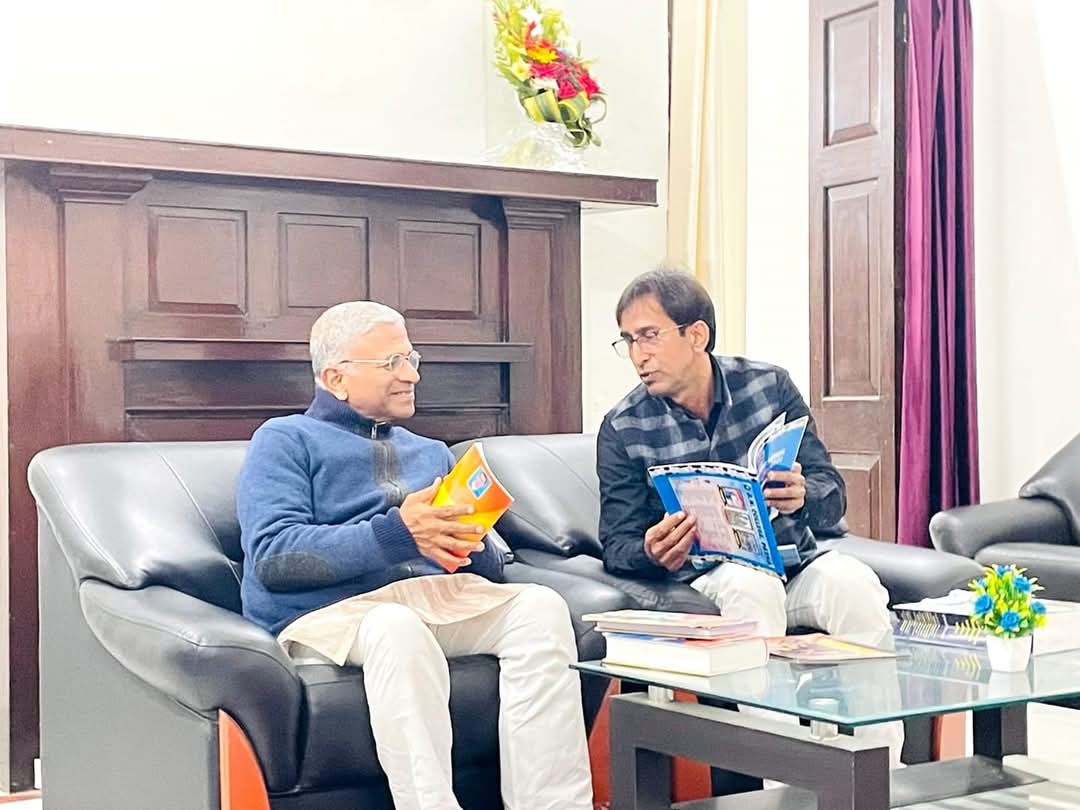“मॉनसून का बदलता मिज़ाज: भारत की कृषि और जल भविष्य पर संकट की आहट”
गरीब दर्शन @ अजय सहाय
भारत में मॉनसून की अनिश्चितता एक गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संकट का संकेत बनती जा रही है, जहाँ वैश्विक तापवृद्धि (Global Warming) और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की बढ़ती तीव्रता ने पारंपरिक मौसमी चक्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश, जहाँ लगभग 55% खेती वर्षा पर निर्भर करती है, वहाँ मॉनसून में होने वाले मामूली बदलाव भी लाखों किसानों की आजीविका, खाद्य उत्पादन और जल संसाधनों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। पिछले 20 वर्षों के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भारत में मानसूनी वर्षा का औसत जहाँ 1951–2000 के बीच 880 मिमी प्रतिवर्ष था, वहीं 2001–2023 के बीच यह घटकर 840 मिमी के आसपास रह गया है, जिसमें क्षेत्रीय असमानताएँ और तीव्र वर्षा के छोटे समय अंतराल में केंद्रित हो जाना, नई चुनौती बन गया है। उदाहरण के तौर पर, 2023 में जून माह में सामान्य से 10% अधिक वर्षा हुई, परंतु जुलाई में 17% की भारी कमी दर्ज की गई, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई। यह असंतुलन न केवल कृषि उत्पादन को घटाता है, बल्कि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) को भी जन्म देता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 2022–23 में धान का उत्पादन 130.29 मिलियन टन से घटकर 127.28 मिलियन टन रह गया और गेहूं उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2023 में अल नीनो (El Niño) की सक्रियता दर्ज की, जिससे मानसून की चाल कमजोर हुई और मध्य तथा उत्तर भारत के कई हिस्सों में सूखा जैसे हालात बन गए। El Niño, जो प्रशांत महासागर के सतही जल के गर्म होने से बनता है, भारत में वर्षा को 15% तक कम कर सकता है, जबकि इसके विपरीत ला नीना (La Niña) के दौरान अधिक वर्षा होती है। वर्ष 2015 और 2009 जैसे वर्षों में जब तीव्र अल नीनो प्रभावी था, तब देशभर में औसत वर्षा क्रमशः 86% और 78% रही, जिससे लगभग 11 राज्यों में सूखा घोषित करना पड़ा। वहीं 2020 और 2021 में ला नीना के कारण अधिक वर्षा हुई, परंतु उस समय भी जल का प्रबंधन चुनौती बना रहा। भारत में जल संकट भी मॉनसून पर निर्भरता के कारण बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत के लगभग 600 जिलों में से 256 जिले “जल संकट ग्रस्त” श्रेणी में आते हैं, जहाँ भूजल का स्तर 10 वर्षों में 40 मीटर से अधिक नीचे चला गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार, देश के 65% से अधिक कृषि क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, जहाँ मानसून की अस्थिरता ने किसानों को बोरवेल आधारित सिंचाई पर निर्भर कर दिया है। वर्ष 2022 में दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति संकट चरम पर पहुँचा, जिससे ‘डे जीरो’ की स्थिति की चेतावनी दी गई। वनों की कटाई (Deforestation), शहरीकरण, जलवायु असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक दोहन मॉनसून प्रणाली को अस्थिर बना रहे हैं। सैटेलाइट आधारित निगरानी से पता चलता है कि भारत में पिछले 20 वर्षों में 2.7 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि का क्षरण हुआ है, विशेषकर मध्य भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जिससे क्षेत्रीय वर्षा चक्र बाधित हुए हैं। उदाहरण के लिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में वर्षा का औसत 12% कम हो गया है। साथ ही, वायु प्रदूषण (aerosols), समुद्री तापमान में वृद्धि, हिमालयी हिमखंडों के पिघलने, और कृषि भूमि के बंजर होने जैसे कारक भी भारतीय मानसून को अप्रत्याशित बना रहे हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वैश्विक तापमान की वृद्धि 2°C के पार जाती है, तो भारतीय मानसून में 25–30% की गिरावट और तीव्र चरम घटनाओं (extreme events) में 50% की वृद्धि हो सकती है। वर्षा के इन असंतुलन के कारण कहीं-कहीं अचानक बाढ़ और कहीं सूखा जैसे परस्पर विरोधी संकट सामने आते हैं, जिससे ग्रामीण आबादी का पलायन, खाद्य असुरक्षा और सामाजिक असंतुलन जन्म लेता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2001–2020 के बीच लगभग 4.5 करोड़ लोग जलवायु संबंधी संकटों के कारण आजीविका के लिए पलायन कर चुके हैं। यही नहीं, मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश घटा है, फसल बीमा की माँग बढ़ी है, और किसान आत्महत्याओं में वृद्धि भी दर्ज की गई है – विशेषकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जल-संवेदनशील फसलों जैसे धान, गन्ना और कपास की जगह सूखा-सहिष्णु फसलों (जैसे ज्वार, बाजरा, दालें) की ओर स्थानांतरण की आवश्यकता है। इसी दिशा में भारत सरकार ने “परम्परागत कृषि विकास योजना”, “अटल भूजल योजना” और “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना” जैसी पहलें शुरू की हैं, परंतु इनके परिणाम सीमित रहे हैं। भारत में कुल 141 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि में से केवल 48% ही सिंचित है, बाकी मॉनसून पर निर्भर है। इसका अर्थ है कि यदि मानसून असफल होता है, तो आधे से अधिक फसल क्षेत्र संकट में आ जाता है। वर्ष 2023 में भी खरीफ फसलों की बुवाई में 8% की गिरावट दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2019 में बाढ़ के कारण 15 राज्यों की 93 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हुईं। यह आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि केवल वर्षा की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी समय-सीमा, स्थानिक वितरण और तीव्रता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मानसून की अनिश्चितता ने नदियों के प्रवाह को भी प्रभावित किया है, जहाँ गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ या तो बाढ़ की स्थिति में पहुँच जाती हैं या फिर गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (IPCC) की छठी रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में मानसून की तीव्रता और अनियमितता भविष्य में और बढ़ेगी, जिससे दीर्घकालीन जल एवं कृषि योजनाएँ असफल हो सकती हैं। अतः समय की माँग है कि भारत जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों, वैज्ञानिक जल प्रबंधन, वन संरक्षण, और ग्रामीण जलस्रोत पुनर्जीवन के प्रति तीव्रता से कार्य करे। मानसून की भविष्यवाणी प्रणाली को और अधिक सटीक बनाना, किसानों को मौसम आधारित चेतावनी देना, और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित करना नितांत आवश्यक है। अंततः, भारत में मानसून केवल जलवायु घटना नहीं है, बल्कि यह कृषि, अर्थव्यवस्था, रोजगार, जल सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर इस अनिश्चितता को विज्ञान, नीति और जन-सहभागिता के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले दशक भारत के लिए जल और खाद्य संकट की त्रासदी बन सकते हैं।